शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम – सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा
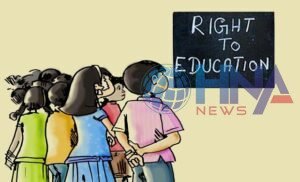
शिक्षा किसी भी देश की प्रगति की नींव होती है। भारत में शिक्षा को सबके लिए सुलभ और समान बनाने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act – RTE), 2009 लागू किया गया। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है।
इस कानून का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा को अनिवार्य बनाना नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सभी वर्गों के बच्चों को समान अवसर देना भी है। यह अधिनियम भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को मज़बूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
आरटीई अधिनियम की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की दिशा में पहला बड़ा कदम 86वें संविधान संशोधन (2002) के तहत उठाया गया, जिसमें अनुच्छेद 21(A) जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया और इसे लागू करने के लिए वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया।
1 अप्रैल 2010 को इस अधिनियम को पूरे देश में लागू किया गया, जिससे भारत विश्व के उन गिने-चुने देशों में शामिल हो गया जहां बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कानूनी अधिकार प्राप्त है।
आरटीई अधिनियम के मुख्य उद्देश्य
✔ हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना।
✔ सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को मुख्यधारा में लाना।
✔ शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
✔ बच्चों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर देना।
✔ सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारना।
आरटीई अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान
1. मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा
इस कानून के तहत 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को बिना किसी शुल्क के मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और अन्य आवश्यक सुविधाएँ भी मुफ्त दी जाती हैं।
2. 25% सीटें वंचित वर्ग के लिए आरक्षित
निजी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अपनी कुल सीटों का 25% वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखना आवश्यक है।
3. अनिवार्य स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर
आरटीई अधिनियम के अनुसार, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएँ जैसे शौचालय, साफ़ पानी, खेल का मैदान, पुस्तकालय, योग्य शिक्षक आदि अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिए।
4. बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोशन (No Detention Policy)
इस अधिनियम के अनुसार पहली से आठवीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। हालांकि, 2019 में इस नीति में बदलाव किया गया और राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वे पाँचवीं और आठवीं कक्षा में परीक्षाएँ आयोजित कर सकते हैं।
5. योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक अनिवार्य
आरटीई अधिनियम के अनुसार, स्कूलों में शिक्षकों की योग्यता और संख्या को निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखना अनिवार्य है। किसी भी स्कूल में अयोग्य शिक्षक नियुक्त नहीं किए जा सकते।
आरटीई अधिनियम के लाभ
🏆 बुनियादी शिक्षा तक सभी बच्चों की पहुँच सुनिश्चित हुई।
🏆 गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिला।
🏆 महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला, जिससे लिंग समानता में सुधार हुआ।
🏆 बच्चों के ड्रॉपआउट रेट में कमी आई।
🏆 स्कूलों में बेहतर सुविधाएँ विकसित की गईं।
आरटीई अधिनियम की चुनौतियाँ
❌ कई निजी स्कूल आरटीई के तहत दाखिले देने में आनाकानी करते हैं।
❌ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है।
❌ शिक्षकों की संख्या और प्रशिक्षण की कमी।
❌ ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की स्थिति में अभी भी सुधार की आवश्यकता।
❌ कुछ राज्यों में आरटीई के प्रावधानों का सही से क्रियान्वयन नहीं हो रहा।
आरटीई को और प्रभावी बनाने के उपाय
✔ आरटीई के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए।
✔ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए।
✔ डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि दूर-दराज़ के बच्चों तक भी अच्छी शिक्षा पहुँच सके।
✔ शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए और उनके लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएँ।
✔ आरटीई को 6-14 साल की जगह 3-18 साल तक के बच्चों के लिए लागू किया जाए।
भविष्य की दृष्टि: क्या आरटीई को और विस्तार देने की जरूरत है?
कई शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आरटीई की समयसीमा (6-14 वर्ष) को बढ़ाकर 3-18 वर्ष कर देना चाहिए ताकि बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकें।
इसके अलावा, आरटीई में डिजिटल शिक्षा को शामिल करना, सरकारी और निजी स्कूलों में समान शिक्षा स्तर सुनिश्चित करना और सभी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है।











